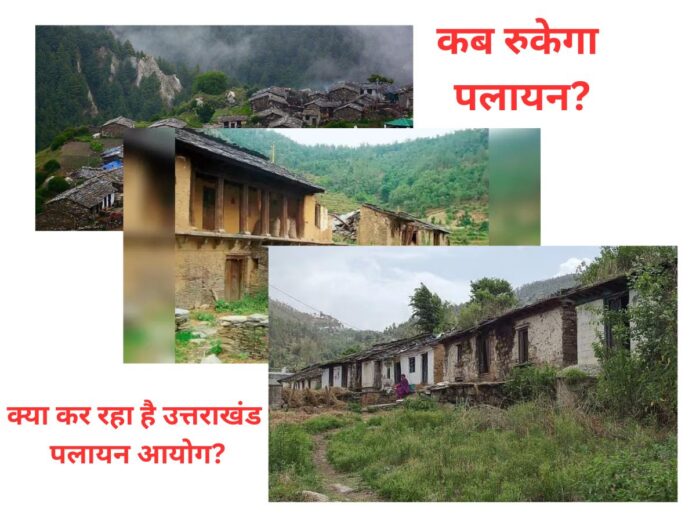उत्तराखंड पलायन आयोग (ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग) की स्थापना 2017 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में हो रहे पलायन के कारणों का अध्ययन करना
और उसे रोकने के लिए प्रभावी समाधान प्रस्तुत करना है। आयोग विशेष रूप से पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर ध्यान केंद्रित करता है।
पलायन रोकने में उत्तराखंड पलायन आयोग की प्रमुख भूमिकाएँ
1. पलायन के कारणों का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करना
उत्तराखंड पलायन आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों और गांवों में विस्तृत सर्वेक्षण कर पलायन के प्रमुख कारणों का अध्ययन किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्टों में बताया कि पलायन के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
रोजगार के अवसरों की कमी
शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव
बुनियादी ढांचे का विकास न होना
कृषि और पशुपालन में गिरावट
आयोग ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन
पलायन को रोकने के लिए आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। इसके तहत, आयोग ने निम्नलिखित क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावनाएँ तलाशी हैं:
पर्यटन और होमस्टे व्यवसाय को बढ़ावा देना
हस्तशिल्प, बागवानी और जैविक खेती को प्रोत्साहन
स्थानीय उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराना
स्वरोजगार योजनाओं को लागू करना
इस दिशा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं को आयोग के सुझावों के आधार पर लागू किया गया है, जिससे लोग अपने गांवों में ही रोजगार प्राप्त कर सकें।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास
आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पतालों का विकास किया जाए। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में
अटल आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया और सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई परियोजनाएँ शुरू कीं।
4. रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना
आयोग ने प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस उनके गांवों में लाने के लिए रिवर्स माइग्रेशन की नीति पर भी कार्य किया है। इसके तहत:
नवीन स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
गांवों में पर्यटन आधारित व्यवसायों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।
कोरोना महामारी के दौरान वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा गया।
5. प्रवासियों से संवाद और नीतिगत सुधार
आयोग उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से लगातार संवाद स्थापित कर रहा है और उनकी राय के आधार पर नीतिगत सुधार कर रहा है। आयोग नवाचार और तकनीकी निवेश को भी प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि राज्य में नई संभावनाएँ उत्पन्न हो सकें।
उत्तराखंड आयोग की उपलब्धियाँ ।
1.पलायन के कारणों का विश्लेषण और डेटा संकलन
उत्तराखंड आयोग की ने राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन के कारणों का गहन अध्ययन किया है। इसके तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे प्रमुख कारणों की पहचान की गई।
आयोग ने विस्तृत सर्वेक्षणों और अनुसंधानों के माध्यम से पलायन से संबंधित आंकड़े संकलित किए, जो नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।
2.नीतिगत सुझाव और योजनाएँ
आयोग ने पलायन रोकने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक, और दीर्घकालिक योजनाओं के प्रस्ताव दिए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, तथा बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।
आयोग के सुझावों के आधार पर राज्य सरकार ने कई योजनाएँ लागू की हैं, जो ग्रामीण विकास में सहायक रही हैं।
3.प्रवासी नागरिकों के साथ समन्वय
आयोग ने राज्य के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया है, ताकि उनके सुझावों और अनुभवों का लाभ उठाया जा सके। इस पहल से न केवल प्रवासियों की राज्य के विकास में भागीदारी बढ़ी है, बल्कि उनके निवेश और विशेषज्ञता का भी उपयोग हो रहा है।
4.नाम परिवर्तन और कार्यक्षेत्र का विस्तार
2022 में, आयोग का नाम “उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग” से बदलकर “पलायन निवारण आयोग” किया गया। इस परिवर्तन से आयोग के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है, जिससे यह पलायन रोकथाम के लिए और अधिक केंद्रित प्रयास कर रहा है।
5.सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग
आयोग ने राज्य सरकार के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास, रोजगार के अवसरों की सृजन, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।